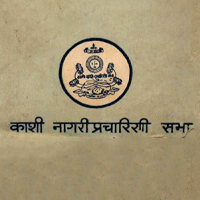नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सूफ़ी लेख
खुसरो की हिंदी कविता - बाबू ब्रजरत्नदास, काशी
तेहरवीं शताब्दी के आरंभ में, जब दिल्ली का राजसिंहासन गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन हो रहा था, अमीर सैफुद्दीन नामक एक सरदार बल्ख़ हज़ारा से मुग़लों के अत्याचार के कारण भागकर भारत आया और एटा के पटियाली नामक ग्राम में रहने लगा। सौभाग्य से सुल्तान शम्सुद्दीन
बिहारी-सतसई की प्रतापचंद्रिका टीका - पुरोहित श्री हरिनारायण शर्म्मा, बी. ए.
(प्रारंभ के कुछ अंश) श्रीगणेशाय नमः श्री महाराजाधिराज महाराजा श्रीसवाई प्रतापसिंह-चंद्रिका लिख्यते छप्पय श्री गनपति तुव चरन सरन द्विज वरुन करुन करि। देवन के दुष दरन करन सुष भरन भाव धरि।। अमरन पददानरन परन धारत बहु भागह। ररत नाम सुभ धरन तरन
बिहारी-सतसई-संबंधी साहित्य (बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर, बी. ए., काशी)
सतसई के क्रम बिहारी की सतसई की जो मूल अथवा, सटीक प्रतियाँ मिलती हैं, उनमें दोहों का पूर्वापर क्रम एक सा नहीं मिलता। किसी में एक दोहा किसी संख्या पर दिखलाई देता है तो अन्य में अन्य संख्या पर। इसका मूल कारण यही है कि बिहारी ने न तो अपने दोहे किसी साहित्यिक
महाकवि सूरदासजी- श्रीयुत पंडित रामचंद्र शुक्ल, काशी।
हिन्दुओं के स्वांतत्र्य के साथ ही साथ वीर-गाथाओं की परंपरा भी काल के अँधेरे में जा छिपी। उस हीन दशा के बीच वे अपने पराक्रम के गीत किस मुँह से गाते और किन कानों से सुनते? जनता पर गहरी उदासी छा गई थी। राम और रहीम को एक बतानेवाली बानी मुरझाए मन को हरा न
खुमाणरासो का रचनाकाल और रचियता- श्री अगरचंद नाहटा
हिंदी के प्राचीन साहित्य का गंभीर अन्वेषण अभी तक बहुत कम हुआ है। फलतः उसके संबंध में बहुत सी भ्रांत बातें प्रचलित हैं एवं कई बातें अनिश्चित रूप से पड़ी है। उदाहरण के लिये, हिंदी-साहित्य के वीरगाथा-काल की जितनी भी रचनाएँ कही जाती हैं उनमें से अधिकांश
मंझनकृत मधुमालती - श्री चंद्रबली पाँडे एम. ए.
जहाँ तक हमें पता है, मंझन की मधुमालती का परिचय पहले पहल हिंदी संसार को स्वर्गीय श्री जगन्मोहन वर्म्मा ने सन् 1912 ई. में स्वसंपादित चित्रावली की भूमिका में लिखा- “जायसी ने पद्मावती में एक जगह अपने पूर्व के रचे हुए कितने ही ग्रंथों का उल्लेख किया है।
नवाब-ख़ानख़ाना-चरितम्- ले. श्री विनायक वामन करंबेलकर
एक सद्यःप्राप्त अज्ञात ग्रंथ संस्कृत के विद्वान राष्ट्रौढवंश-महाकाव्य के रचयिता रुद्र कवि के नाम से परिचित है। इस महाकाव्य के संपादक का मत है कि रुद्र कवि ही जहाँगीरचरितम् के भी रचियता थे। परंतु उनकी इस तृतीय कृति का अभी तक किसी को पता भी नहीं था।
खुसरो की हिंदी कविता - बाबू ब्रजरत्नदास, काशी
तेहरवीं शताब्दी के आरंभ में, जब दिल्ली का राजसिंहासन गुलाम वंश के सुल्तानों के अधीन हो रहा था, अमीर सैफुद्दीन नामक एक सरदार बल्ख़ हज़ारा से मुग़लों के अत्याचार के कारण भागकर भारत आया और एटा के पटियाली नामक ग्राम में रहने लगा। सौभाग्य से सुल्तान शम्सुद्दीन
बीसलदेव रासो- शालिग्राम उपाध्याय
डा. तारकनाथ अग्रवाल द्वारा संपादित यह कृति कलकत्ता विश्वविद्यालय से डी. फिल. उपाधि के हेतु स्वीकृत शोधप्रबंध है। इससे पहले यह सर्वप्रथम नागरीप्रचारिणी सभा, काशी से भी सत्यजीव वर्मा द्वारा संपादित होकर सं. 1982 में इसी नाम से, तथा हिंदी परिषद विश्वविद्यालय,
अभागा दारा शुकोह - श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव
सोमवार 20 मार्च सन् 1615 की रात्रि में, मेवाड़ की सफलता के एक मास पश्चात्, भारतवर्ष की ऐतिहासिक नगरी अजमेर में राजकुमार खुर्रम की प्रियतमा मुमताज महल ने शाहजहाँ के सब से प्रिय, सबसे विद्वान् पर सबसे अभागे द्वारा शुकोह को जन्म दिया। बाबा का दिया हुआ ‘मुहम्मद
संत कबीर की सगुण भक्ति का स्वरूप- गोवर्धननाथ शुक्ल
कबीर के संपूर्ण वाङ्मय का रहस्य सत्यं शिवं सुंदरं की साधना एवं उपासना है। उनकी यह उपासना प्रमुख रूप से मानसी और गौण रूप से वाङ्मयी थी। जिस प्रकार अपने समय के प्रचलित सभी काव्यरूपों को अपना कर वे अपनी एक निराली काव्यशैली के स्रष्टा बन गए उसी प्रकार अपने
पदमावत के कुछ विशेष स्थल- श्री वासुदेवशरण
मलिक मुहम्मद जायसी कृत पदमावत की भाषा ऊपर से देखने पर बोलचाल की देहाती अवधी कही जाती है, किंतु वस्तुतः वह अत्यंत प्रौढ़, अर्थ-संपत्ति से समर्थ शैली है। अनेक स्थानों पर जायसी ने ऐसी ऐसी श्लेषात्मक भाषा का प्रयोग किया है जिसके अर्थ लगातार कई दोहों तक एक
कदर पिया- श्री गोपालचंद्र सिंह, एम. ए., एल. एल. बी., विशारद
हिंदी-संसार अपने मुसलमान कवियों का सदा ऋणी रहेगा। उन अनेक मुसलमान कवियों में, जिन्होंने अपनी सरस रचनाओं से हिंदी का उपकार किया है, लखनऊ के सुविख्यात मिर्जा वाला कदर साहब का भी नाम उल्लेखनीय है। आप का निजी नाम वज़ीर मिर्जा था, पर अपनी समस्त उपाधियों सहित
मीरा से संबंधित विभिन्न मंदिर- पद्मावती शबनम
राजस्थान की भक्तिमती नारी मीराबाई की ख्याति देश के कोने कोने में व्याप्त है। जितनी ही अधिक इनकी प्रशस्ति है उतना ही उलझा हुआ इनका जीवनवृत्त है। इतना ही नहीं, इस अपूर्व प्रशस्ति के ही कारण प्राप्त सामग्री में किंवदंतियों की संख्या विशेष है। मीरा बाई द्वारा
रामावत संप्रदाय- बाबू श्यामसुंदर दास, काशी
हिंदी साहित्य का इतिहास तीन मुख्य कालों में विभक्त किया जा सकता है- प्रारंभ काल, मध्य काल और उत्तर काल। प्रारंभ काल का आरंभ विक्रम संवत् 800 के लगभग होता है, जब इस देश पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हो गए थे पर वे स्थायी रूप से यहाँ बसे नहीं थे। यह युग
उमर खैयाम की रुबाइयाँ (समीक्षा)- श्री रघुवंशलाल गुप्त आइ. सी. एस.
जिस दिन इंगलैंड के रसज्ञ कवि रोजेटी ने रुबाइयात् आव् उमर खैयाम उसके विक्रेता से- दूकान के बाहर डाली हुई, न बिकनेवाली पुस्तकों के ढेर में से- एक पेनी (एक आने) में बड़े कौतूहल से खरीदी और फिर रसाप्लुत हो अपने सभी मित्रों को खरिदवाई, उस दिन विश्व में उमर
मीरां के जोगी या जोगिया का मर्म- शंभुसिंह मनोहर
मीरां के कुछ पदों में जोगी या जोगिया का उल्लेख हुआ है। उदाहरणार्थ- 1. जोगी मत जा, मत जा, पांइ परुँ मैं तेरी चेरी हो। प्रेम भगति के पैंडो म्हारो, हमको गैल बताजा।। 2. जोगिया जी आज्यो जी इण देस। नैणज देखूँ नाथ नै, धाइ करुँ आदेस।। 3. जोगिया से
चतुर्भुजदास की मधुमालती- श्री माताप्रसाद गुप्त
चतुर्भुजदास कृत मधुमालती हिंदी की एक प्राचीन प्रेम-कथा है जो विशुद्ध भारतीय शैली में लिखी गई है। चतुर्भुजदास नाम के एक से अधिक साहित्यकार हुए हैं, जिनमें से एक तो अष्टछाप के प्रसिद्ध भक्त थे, और मधुमालती नाम की भी एक से अधिक रचनाएँ मिलती है, इसलिये हमारे
जायसी का जीवन-वृत्त- श्री चंद्रबली पांडेय एम. ए., काशी
उपोद्धात ग्रियर्सन साहब एवं पंडित सुधाकर द्विवेदी ने मलिक मुहम्मद जायसी के उद्धार की जो चेष्टा की थी उसके विषय में श्रद्धेय शुक्लजी का कथन है- “इसी प्रकार की भूलों से टीका भरी हुई हैं। टीका का नाम रखा गया है सुधाकर-चंद्रिका। पर यह चंद्रिका हैं कि घोर
कुतुबनकृत मृगावती के तीन संस्करण- परशुराम चतुर्वेदी
हिंदी के सूफी कवियों की अभी तक उपलब्ध प्रेमगाथात्मक रचनाओं में कुतुबनकृत मृगावती को, कालक्रमानुसार, द्वितीय स्थान दिया जाता आया है और मुल्ला दाऊद की चंदायन को भी, इस तरह की प्रथम कृति होने का श्रेय परदान किया गया है। इन दोनों के रचनाकाल में लगभग सवासौ
कबीर साहब और विभिन्न धार्मिक मत- श्री परशुराम चतुर्वेदी
कबीर साहब का आविर्भाव विक्रम की पंद्रहवी शताब्दी में हुआ था। उस समय भारत में अनेक मत-मतांतर प्रचलित थे और विभिन्न संप्रदायों के जटिल विधानों तथा उनके अनुयायियों के परस्पर-विरोधी आचरणों की अंधाधुंध में वास्तविक धर्म का रहस्य जानना कठिन हो रहा था। फलतः
अबुलफजल का वध- श्री चंद्रबली पांडे
वीर और विवेकी अल्लामा अबुलफजल के वध के विषय में इतिहासों में जो कुछ पढ़ा वह गले के नीचे न उतरा, पर उसे सत्य के अतिरिक्त और कोई उपाय भी तो न था। इसी उलझन में था कि महाकवि केशवदास का वीरसिंहदेवचरित हाथ लगा। बडे चाव से पढ़ा। सोचा स्यात् कहीं से कुछ और हाथ
संत रोहल की बानी- दशरथ राय
हिंदी सब कालों में समस्त भारत में समान रूप से अपना स्थान बनाए जनसंपर्क की भाषा बनी रही हैं और भारत के समस्त प्रदेशों ने हिंदी के विकास में अपना पूर्ण योगदान दिया है। राजनीतिक मंच ने आज हिंदी के प्रति उदासीनता ग्रहण कर ली है और प्रांतीयता की भावना के
आलोचना- महाकवि बिहारीदास जी की जीवनी-मयाशंकर याज्ञिक
ब्रजभाषा-मर्मज्ञ साहित्य-सेवी बाबू जगन्नाथदास रत्नाकर ने स्वरचित “बिहारी-रत्नाकर” नाम की एक बड़ी विद्वत्तापूर्ण टीका बिहारी-सतसई पर प्रकाशित की है। इस टीका की प्रशंसा बड़े बड़े विद्वानों ने की है। उसके विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता ने की है। उसके
पदमावत की लिपि तथा रचना-काल- श्रीचंद्रबली पांडेय, एम. ए., काशी
पदमावत का अध्याय करते करते जब हम उसकी कथा के उपसंहार में पहुँचते हैं तब हमारी कुछ विचित्र स्थिति हो जाती है। उस समय हम एक ऐसी परिस्थिति में पड़ जाते हैं जिसकी हमें संभावना भी नहीं हुई थी। हम यह नहीं कहते कि जायसी ने उस स्थल पर जो कुछ लिख दिया है वह अनुचित
कबीर जीवन-खण्ड- लेखक पं. शिवमंगल पाण्डेय, बी. ए., विशारद
कबीर की जीवन-घटना साधारण नहीं है। वह पद पद पर आलौकिकता से पूर्ण है। आरम्भ से अन्त तक आश्चर्यमय है। जिती ही उनकी उत्पत्ति संदिग्ध और अज्ञात है, उतना ही उनका मरण और उनकी जीवन-व्यवस्था भी। सत्यतः उनके जीवन की कोई ऐसी घटना नहीं है, जिसमें दैविकता और पारलौकिकता